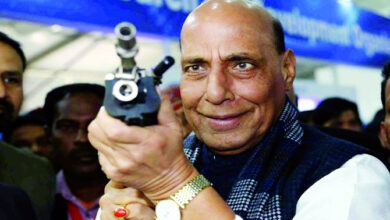जातिवादी सियासत में खत्री-मिस्त्री की ‘बलि’

देश के धुरंधर कांग्रेसियों का मिशन यूपी
संजय सक्सेना
 वर्ष 2017 में जिन पांच राज्यों (यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड) में विधान सभा चुनाव होने हैं उसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब प्रमुख है। पंजाब में अकाली दल-बीजेपी की गठबंधन वाली तो यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार है। स्वभाविक रूप से दोनों ही जगह सत्ता विरोधी माहौल बना हुआ है। पंजाब में नशाखोरी और यूपी में बिगड़ी कानून व्यवस्था को विरोधियों ने सत्तारूढ़ दल के खिलाफ मजबूत सियासी हथियार बना रखा है। पंजाब से कांग्रेस को काफी उम्मीद है तो उत्तर प्रदेश उसके लिये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी को जीते बिना दिल्ली नहीं जीती जा सकती है। इसीलिये दोंनों ही राज्यों में विधान सभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तेजी चौकाने वाली है। पंजाब की सियासी जंग कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के सहारे फतह करना चाहती है तो यूपी के लड़ाई वह रणनीतिकार प्रशांत किशोर और गुलाम नबी आजाद जैसे आयातित (प्रदेश के बाहर के) नेताओं के सहारे जीतना चाहती है। आलाकमान को यूपी में एक अदद ऐसा चेहरा नहीं मिल रहा है जिसके सहारे विधान सभा चुनाव जीता जा सके। मौके की नजाकत को भांप कर यूपी फतह करने के लिये कांग्रेस आलाकमान ने देश भर के अपने तमाम धुरंधरों को मिशन यूपी पर लगा दिया है।
वर्ष 2017 में जिन पांच राज्यों (यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड) में विधान सभा चुनाव होने हैं उसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब प्रमुख है। पंजाब में अकाली दल-बीजेपी की गठबंधन वाली तो यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार है। स्वभाविक रूप से दोनों ही जगह सत्ता विरोधी माहौल बना हुआ है। पंजाब में नशाखोरी और यूपी में बिगड़ी कानून व्यवस्था को विरोधियों ने सत्तारूढ़ दल के खिलाफ मजबूत सियासी हथियार बना रखा है। पंजाब से कांग्रेस को काफी उम्मीद है तो उत्तर प्रदेश उसके लिये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी को जीते बिना दिल्ली नहीं जीती जा सकती है। इसीलिये दोंनों ही राज्यों में विधान सभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तेजी चौकाने वाली है। पंजाब की सियासी जंग कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के सहारे फतह करना चाहती है तो यूपी के लड़ाई वह रणनीतिकार प्रशांत किशोर और गुलाम नबी आजाद जैसे आयातित (प्रदेश के बाहर के) नेताओं के सहारे जीतना चाहती है। आलाकमान को यूपी में एक अदद ऐसा चेहरा नहीं मिल रहा है जिसके सहारे विधान सभा चुनाव जीता जा सके। मौके की नजाकत को भांप कर यूपी फतह करने के लिये कांग्रेस आलाकमान ने देश भर के अपने तमाम धुरंधरों को मिशन यूपी पर लगा दिया है।
कांग्रेस से जुड़ी खबरें मीडिया में सबसे अधिक सुर्खियां बटोर रही हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जब कांग्रेस खेमे से कोई चौका देने वाली खबर न आती हो। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत कुमार (पीके) जब से कांग्रेस के साथ आये हैं तब से कांग्रेस में कुछ अधिक बेचैनी देखने को मिल रही है। इस पर गुलाम नबी आजाद को यूपी का प्रभारी बनाया जाना ‘सोने पर सुहागा’ साबित हो रहा है। उम्मीद है कि देर-सबेर यूपी कांग्रेस को निर्मल खत्री की जगह नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जायेगा। सब कुछ चुनावी बिसात के लिये किया जा रहा है। कांग्रेसियों की तरफ से माहौल कुछ ऐसे बनाया जा रहा है, जैसे वह (कांग्रेस) सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार हो। यह स्थिति तब है जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वादों-दावों को कोई ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता है। इसकी वजह पर जाया जाये तो लगता है कि कांग्रेस आलाकमान में निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। फैसले लेने की प्रक्रिया इतनी लंबी और सुस्त होती है कि जब तक फैसला लिया जाता है तब तक स्थितियां बहुत बदल जाती हैं। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री को हटाने के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। निर्मल खत्री जातीय समीकरण के हिसाब से कांग्रेस के लिये फायदेमंद नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के भीतर इस बात पर सैद्धांतिक सहमति हो जाने के बाद भी दो साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया लेकिन नये प्रदेश अध्यक्ष की तलाश अभी तक नहीं पूरी हो पाई है। हालात यह थी कि प्रदेश अध्यक्ष (अब निवर्तमान) निर्मल खत्री को कई बार मीडिया के सामने आकर कहना पड़ा था कि उन्हें हटाया नहीं गया है।
आश्चर्यजनक तो यह भी था कि निर्मल के इस्तीफा देने के बाद भी शीर्ष नेतृत्व ने इस खबर को सार्वजनिक करने में काफी टाइम लगा दिया था। एक तरफ निर्णय लेने में देरी और उस पर कांग्रेस के पास जनाधार वाले नेताओं की कमी। कांग्रेस के लिये स्थायी समस्या बनती जा रही है। जो नेता बचे भी हैं, वे आपस में ही सिर फुटव्वल कर रहे हैं। यूपी में तो कांग्रेस के कई प्रभारियों ने ही जिन्हें पार्टी की दिशा-दशा सुधारने के लिये भेजा गया था, पार्टी के भीतर अपने स्तर पर गुटबाजी की हवा देने का काम किया है तो कुछ प्रभारी पहले से चली आ रही गुटबाजी को खत्म करने में नाकाम रहे है। हाल ही में प्रदेश प्रभारी पद से हटाये गये मिस्त्री इसकी मिसाल थे। नेताओं के अभाव के कारण संगठन भी कमजोर होता जा रहा है। किसी भी संगठन के लिए जो बूथ लेवल स्तर का संगठनात्मक ढांचा होता है, वह एक तरफ से पार्टी या संगठन की जान होता है। कांग्रेस में यह दम तोड़ा जा चुका है। कांग्रेस के फ्रंटल संगठनों ने भी अपना औचित्य खो दिया है। वे जिस मकसद को लेकर बनाए गए हैं उसके अनुरूप काम ही नहीं कर रहे हैं। नतीजतन, वोटर में तब्दील हुआ छात्र वर्ग, युवा और महिलाएं जो अब बड़े वोट बैंक में तब्दील हो चुकी है। उनके बीच कांग्रेस की कोई पहचान ही नहीं दिखती।
बात अतीत की की जाये तो करीब तीन दशकों से यूपी की सियासत में हासिये पर चल रही कांग्रेस कभी यूपी की सिरमौर हुआ करती थी। देश को कई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देने वाली कांग्रेस ने लम्बे समय तक प्रदेश पर राज किया परंतु जब से यूपी में मंडल-कमंडल की राजनीति का उद्भव हुआ तब से कांग्रेस का रुतबा क्षेत्रीय दलों ने हासिल कर लिया। मंडल-कमंडल के दलदल से बड़ा-छोटा कोई नेता बच नहीं पाया। मंडल-कमंडल के अलावा भी 1984 से 1990 के दौरान ऐसे कई सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए जिनकी वजह से कांग्रेस की जमीन खिसकती गई। कांग्रेस ने मंडल-कमंडल की राजनीति में अपने आप को फिट करने की काफी कोशिश की, मगर उसकी सियासी हांडी चढ़ नहीं पाई।
वर्ष 1989 में भारतीय राजनीति में जब नए युग की शुरुआत हुई और कांग्रेस के कमजोर पड़ने और क्षेत्रीय दलों के उभार के बाद केन्द्र और राज्य की राजनीति में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो गया। मंडल-कमंडल की राजनीति में, मंडल की राजनीति के नायक तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने तो मंडल की काट के लिये कमंडल (अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का मुद्दा) को हवा देने में भगवा खेमा आगे रहा। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए वी पी सिंह ने मंडल आयोग की आरक्षण संबंधित सिफारिशें लागू करके भले ही नौकरियों में नए अवसरों के द्वार खोल दिये थे, परंतु वीपी सिंह के इस कदम की ऊपरी जाति के लोंगो ने तीखी प्रतिक्रिया दी। जगह-जगह माहौल हिंसक होने लगा। आरक्षण विरोधी सड़क पर उतर आये। यही वजह थी बुद्धिजीवी कहने लगा कि सामाजिक न्याय के नाम पर वी पी सिंह ने सिर्फ जाति विभेदों को बढ़ावा दिया। देशभर में छिड़ी आरक्षण की बहस ने पिछड़े वर्ग को अपनी पहचान का एहसास दिलाया। इस पहचान के एहसास ने उन लोगों का काम आसान कर दिया जो इस वर्ग को राजनीति में लाना चाहते थे। पिछड़े वर्ग को अच्छी शिक्षा, रोजगार के वायदे के साथ कई नई-नई पार्टियां इस दौर में अस्तित्व में आयीं। नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव आदि तमाम नेता इसी सियासत की देन थे।
मंडल-कमंडल की सियासत में मंडल और कमंडल दोनों की ही राजनीति करने वालों को फायदा हुआ। सिर्फ कांग्रेस को ही नुकसान उठाना पड़ा। उसके पास इस स्थिति से मोर्चा लेने के लिये न तो इंदिरा गांधी मौजूद थी, न संजय और राजीव गांधी। कांग्रेस का वोट बैंक तितर-बितर हो गया। जो मंडल-कमंडल की काट कर सकें, कांग्रेस में ऐसे नेताओं को आकाल पड़ गया, जिसका खामियाजा कांग्रेस को सत्ता गंवा कर चुकाना पड़ा। जब नेता नहीं बचे तो कार्यकर्ता भी मायूस होकर घरों में बैठ गया। यूपी में कांग्रेस को सबसे अधिक नुकसान हुआ। जिस कांग्रेस के 1980 में 309 और 1985 में 269 विधायक (425 में से) थे 1989 में उनकी संख्या 94 पर सिमट गई। इसके बाद यूपी में कांग्रेस कभी उभर नहीं पाई।
आज की तारीख में कांग्रेस के मात्र 28 (403 में से) विधायक हैं। बात वोट प्रतिशत की कि जाये तो 1993 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मात्र 15.1, 1996 में 29.1, 2002 में महज 08.9, 2007 में 08.8 और 2012 में 11.6 प्रतिशत मत ही मिले। 2012 में कांग्रेस की स्थिति में दो-तीन प्रतिशत का सुधार तब आया था, जबकि राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वह वन मैन आर्मी की तरह सूबे में प्रचार कर रहे थे। उन्हीं के इशारे पर चुनावी रणनीति बनाई जा रही थी और उनकी पसंद के मुद्दों को हवा दी जा रही थी।
बहरहाल, अतीत से निकल पर वर्तमान में आया जाये तो कांग्रेस के लिये अभी भी हालात कुछ ज्यादा बदले हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सिवाय कुछ मोहरों को इधर से उधर किये जाने के। कांग्रेस आज भी नेतृत्व के अभाव से जूझ रहा है। चुनाव की बेला हो और उसके युवराज राहुल गांधी विदेश सैर करने को निकल जायें तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शीर्ष नेतृत्व के प्रति कांग्रेसियों की क्या सोच होगी? हो सकता है यह लेख आप तक पहुंचे तब तक राहुल गांधी स्वदेश आ गये हों, लेकिन राहुल के विदेश दौरे पर चर्चा तो छिड़ी ही रहेगी। राहुल का विदेश दौरा इसलिये और भी सुर्खिंयों में है क्योंकि इससे पहले भी वह कई बार संकट के समय कांग्रेस को मझधार में छोड़ कर विदेश जा चुके हैं।
इसके बावजूद अच्छी बात यह है कि राहुल भले की कांग्रेस के लिये अभी तक ‘मील का पत्थर’ नहीं बन पाये हों लेकिन कांग्रेसियों को हमेशा उनसे काफी उम्मीद रहती है। यह और बात है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ऐसा नहीं सोचते हैं। कुछ समय पहले कांगेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हमने भ्रम पाल रखा है कि कोई शख्स छूते ही सब कुछ बदल जाएगा तो यह अपने आप को धोखा देना है। उनका इशारा राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपे जाने की मांग की तरफ था। उनका कहना था कि कांग्रेस को संकट से उबारने के लिए सभी को सामूहिक रूप से, ईमानदारी के साथ, एक ठोस एक्शन प्लान लेकर प्रयास करने होंगे। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल यह है कि वहां जयराम रमेश जैसी सोच रखने वाले कम ही लोग है और दस जनपथ के अलावा किसी के पास कोई अधिकार भी नहीं है। इसीलिये कांग्रेस न तो केन्द्र और न प्रदेश की राजनीति में उबर पा रही है। लोकसभा चुनाव के दो साल हो गए हैं। यह वक्त किसी भी पार्टी के हार की हताशा से उबर कर मुकाबले की तैयारी के लिये पर्याप्त माना जा सकता हैं, लेकिन कांग्रेस इन दो सालों में संभलने के बजाय और ज्यादा गहरे गड्ढे में गिरती जा रही है। उसका संकट खत्म होने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है।
लब्बोलुआब यह है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत नेतृत्व के अभाव, निर्णय लेने की क्षमता में कमी, जनाधार वाले नेताओं के न रहने या हासिये पर कर दिये जाने, संगठनात्मक ढांचा कमजोर होने जैसी समस्याओं से जूझ रही है। इसी के चलते उसे समझ में ही नहीं आता है कि किस मुद्दे को कैसे हैंडिल किया जाये। इन्हीं खामियों की वजह से कांग्रेस हो-हल्ला वाली पार्टी में तब्दील होती जा रही है। कांग्रेस को अपने पुराने दिन लौटाने हैं तो उन्हें दुष्यंत कुमार की कविता की दो पक्तियां, ‘सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलना चाहिए।’ को बार-बार दोहराना होगा। उसे 2002 से आगे बढ़कर और सूटबूट एवं उद्योगपतियों की सरकार जैसे जुमलों को दरकिनार करके आगे की सोचना होगा।
इसकी शुरुआत के लिये अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव से बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता है और यूपी को बिना जातीय समीकरण दुरुस्त किये नहीं जीता जा सकता है। यह भी एक सच्चाई है। इसीलिये कांग्रेस आलाकामान अपने परम्परागत ब्राह्मण-मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुट गई है। ब्राह्मण-मुस्लिम वोट बैंक साधने की चाहत ने ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री और यूपी प्रभारी मधुसूदन मिस़्त्री की ‘सियासी बलि’ ले ली। चर्चा यही है कि ब्राह्मणों को साधने के लिये कांग्रेस अपने ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बना सकती है। मुसलमानों को लुभाने के लिये गुलाम नबी आजाद को पहले ही यूपी का प्रभारी बनाया जा चुका है। ल्ल