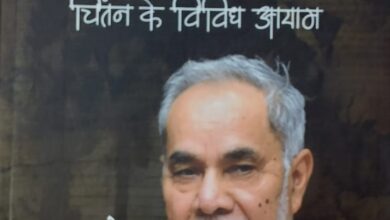गौरैया बनकर सार्थक रचनाएं अब फुर्र हो गईं

नई सदी में साहित्य दिशाहीन हो चुका दिखता है। न अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है और न पढ़ा जा रहा है। बाजार में ज्यादातर हल्के और औसत किस्म के लेखक हैं और कुछ फर्जी किस्म के बेस्ट सेलर किताबों केनाम हैं। फेसबुक पर नई पीढ़ी के कथित साहित्यकारों के कुछ गुट बन गए हैं जो एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने में व्यस्त हैं। पुरानी पीढ़ी के रचनाकार सोशल मीडिया की अराजकता से दूर अपनी दुनिया में गुम हो गए हैं। न अच्छी सहित्यिक पत्रिकाएं हैं और न राजेन्द्र यादव या रवीन्द्र कालिया जैसे साहित्य संपादक। आलोचना नाम की तो संस्था ही खत्म हो चुकी है। नई सदी भी पच्चीस साल की युवा हो गई लेकिन साहित्य में वो ताज़गी नदारद है। 21वीं सदी के लेखन पर चर्चित लेखक व उपन्यासकार दयानंद पांडेय से दयाशंकर शुक्ल सागर की बातचीत।
सवाल- 21वीं सदी के पिछले ढाई दशक में हिंदी साहित्य के कथ्य, उसकी भाषा और शिल्प में किस तरह के बदलाव देखते हैं?
-कथ्य, भाषा और ट्रेंड में कोई आमूलचूल या आसमानी बदलाव नहीं है। हां, भटकाव बहुत बढ़ा है। बहुत ज़्यादा बढ़ा है। असहमति का पाखंड बढ़ा है। असल में हम साहित्य को संवाद के लिए जानते हैं, वाद के लिए नहीं। वाद कोई भी हो, आपको खूंटे से बांध देता है। वाद होता है तो प्रतिवाद भी होता है। तब संवाद की सांस फूलने लगती है। जबकि संवाद समय से मुठभेड़ करना सिखाता है। संवाद बहती नदी है, जो पानी को साफ़ करती हुई बहती है। स्वस्थ समाज का निर्माण यही साहित्य करता है। इसीलिए साहित्य युग चिंतक ही नहीं, भविष्यद्रष्टा भी होता है।
सवाल- राजेन्द्र यादव के युग में साहित्य पर वामपंथ का गहरा प्रभाव दिखता था। हंस पर स्त्री-विमर्श और दलित-विमर्श के नाम पर काफी अराजकता फैलाने के इल्ज़ाम लगे। इसी कारण हंस हमेशा चर्चा में भी रहा। अब वामपंथ का यह प्रभाव कितना शेष है?
-सच कहें तो वामपंथ और उसका प्रभाव कपूर की तरह उड़ता जा रहा है। वामपंथ हो, हिंदुत्व हो या कोई और विचारधारा। साहित्य, रचना और आलोचना में जब भी कोई विचारधारा घुसती है, वह साहित्य, वह रचना, वह आलोचना कूड़ा हो जाती है, दो कौड़ी की हो जाती है। किसी दरबारी रचना से भी ज़्यादा ख़तरनाक है यह विचारधारा वाली रचना। फिर हिंदी में तो वामपंथ का बाक़ायदा इस्लामीकरण हो चुका है। मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ़ हिंदी साहित्य में निल बटा सन्नाटा है। बल्कि कई दफा तो समर्थन में खड़ा दिखता है। रही बात राजेंद्र यादव की तो हिंदी में उन्होंने नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी जैसों की तानाशाही को चुनौती देकर नए खिड़की, दरवाजे खोले। इस बहाने लोकतांत्रिक होने का भ्रम फैलाया। असल में राजेंद्र यादव को हम जब याद करते हैं तो पाते हैं कि बरास्ता हंस उन्होंने नए खिड़की, दरवाज़े खोलने के बहाने जातीय नफ़रत के बीज ज़्यादा बोए। साहित्य में नफ़रत के लिए कोई जगह नहीं होती।
सवाल- जातीय नफ़रत तो सदियों से मौजूद है, साहित्य ने सिर्फ उसे कुरेदने का काम किया। यही तो साहित्य का काम है न?
-ऐसा नहीं है, प्रेमचंद, रेणु या राही मासूम रज़ा ने जातीय नफ़रत के बीज नहीं बोए। कहीं किसी रचना में नहीं।
सवाल- तो साहित्य से आप मुहब्बत की दुकान चलाने की उम्मीद कर रहे हैं?
-नहीं, इसे समझें। आप पुराने पन्ने पलटें तो पाएंगे कि रामायण हो, महाभारत हो गीता हो, यह सभी अपनी फ़िलॉसफ़ी के लिए जाने जाते हैं, विष वमन या नफ़रत के लिए नहीं। आप आधुनिक युग में आएं तो पाएंगे कि टालस्टॉय हों या टैगोर,यह सभी अपनी रचनाओं में फ़िलॉसफ़ी के लिए, मनुष्यता से प्यार और पूजा के लिए ही जाने जाते हैं। पर बाद के समय में वामपंथ के विष ने साहित्य में आइडियोलॉजी की नर्सरी लगा दी। राजेंद्र यादव सरीखे लोगों ने इस नर्सरी को लपक लिया। अंतत: साहित्य में नफ़रत की रोशनाई छिड़क कर विचारधारा का विष बो कर साहित्य को कूड़ेदान बना दिया।
सवाल- इसे आप इतने कन्विक्शन से कैसे कह सकते हैं?
-आप देखिए न। राजेंद्र यादव के हंस ने ऐसी कोई कालजयी रचना नहीं पेश की जैसी टालस्टॉय या टैगौर की रचनाओं ने की। हंस में समुद्र की लहरों की तरह उछलती हुई रचनाएं आईं और समुद्र में ही डूब गईं। दुष्यंत और धूमिल की रचनाओं की तरह लोगों के दिल-दिमाग़ पर छा नहीं सकीं। मुहावरा बनकर ज़ुबान पर चढ़ नहीं सकीं। प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रेणु, अज्ञेय, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, मनोहर श्याम जोशी की रचनाओं की तरह तरह मन में बस नहीं सकीं। प्रेमचंद जब पूड़ी-तरकारी लिखते हैं, तब पढ़ते समय आप के मुंह में भी पूड़ी-तरकारी आ जाती है। प्रेमचंद की यही ताकत है। शरतचंद जब किसी स्त्री की कथा लिखते हैं तो वह स्त्री आपके दिल में आकर बस जाती है। कथा का मर्म यही होता है।
सवाल- पिछले कोई दस-बारह साल में जैसे हिन्दुत्व का उफान आया है, उसका वर्तमान साहित्य पर कोई ज्यादा असर नहीं दिखता। तो राजनीति में वामपंथ के हाशिए पर आने के बाद साहित्य किस रास्ते चल निकला है?
-साहित्य में हिंदुत्व ही नहीं आया। उफान की बात तो बहुत दूर की बात है। अब अगर राम कथा, कृष्ण कथा या विवेकानंद की कथा लिखने को कोई हिंदुत्व मान लेता है तो उसकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है।
सवाल- क्या यह दौर उत्तर आधुनिक युग का एक्स्टेंशन है?
-साहित्य सर्वदा आधुनिक होता है। अद्यतन होता है। उपेक्षित और वंचित के पक्ष में होता है। शोषक के खिलाफ़, शोषित के पक्ष में होता है। यह उत्तर आधुनिक वगैरह यूरोपीय शब्दावली है। बहुत खोखली है। ढकोसले बाजी है, पाखंड है।
सवाल- कागज़ पर छपने वाली साहित्यिक पत्रिकाओं का दौर गुजर चुका है। डिजिटल पत्रिकाओं के इस दौर में क्या नए साहित्य का सही मूल्यांकन हो पर रहा है?
-साहित्यिक पत्रिकाएं सर्वदा हाशिए पर ही रही हैं। डिजिटल हो या प्रिंट में। और ये भी हाशिए पर हैं। जो भी हो प्रिंट का समय सर्वदा जीवित रहेगा, लेकिन यह सही है कि तकनीक ने बहुत कुछ बदल दिया है। सूचना और प्रसार की इसकी ताक़त अनूठी है। एक क्लिक पर पूरी दुनिया उपस्थित है। पर कोई मोटी किताब, कोई महत्वपूर्ण रचना को प्रिंट में पढ़ना ही सुविधाजनक होता है। सुखद और सुखकर होता है, डिजिटल में नहीं।

सवाल- यह आपके निजी विचार हो सकते हैं। नई पीढ़ी के लिए डिजिटल पर पढ़ना ज्यादा आसान है। सारा का सारा सोशल मीडिया डिजिटल है और खूब पढ़ा जा रहा है?
-हां, यह मेरा निजी विचार ही है। बहुत से पाठकों ने मुझे भी बताया है और बारंबार बताया है कि मेरे कई उपन्यास यात्राओं में मोबाइल पर पढ़े हैं लेकिन क्या कोई पूरी रामायण, महाभारत या फिर टालस्टॉय का वॉर एंड पीस डिजिटल पर पढ़ सकता है? गीता पढ़ सकता है? हो सकता है पढ़ लेता हो। पर मुझे मुश्किल लगता है। सत्यनारायण की कथा नहीं हैं यह रचनाएं कि आप डिजिटल पर पढ़ लें या सुन लें। यह सिर्फ उदाहरण है। ऐसी अनेक रचनाएं हैं जो पढ़ने के लिए एक निश्चित अवकाश मांगती हैं। मन मांगती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा, मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी, यशपाल का झूठा सच आदि अनेक रचनाएं हैं जिन्हें आप डिजिटल पर संजीदा हो कर पढ़ने में सहज न पाएं ख़ुद को। बाक़ी नई पीढ़ी का क्या है, वह तो मोबाइल पर सात घंटे, आठ घंटे की वेब सीरीज भी देख ही रही है।
सवाल- नई सदी के बीते दो दशकों की कहानियों, उपन्यासों, कविताओं के बारे में आप क्या कहेंगे ?
-दुनियाभर की सभी भाषाओं में बहुत महत्वपूर्ण रचा गया है, रचा जा रहा है। फिर भी अगर आप हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं तो इस दो दशक में ऐसी कोई बड़ी रचना मेरी नज़र में नहीं आई है जिसे लोग लपक कर, खोज कर पढ़ें। न ग़द्य में, न पद्य में। ऐसी रचना, जिसको पढ़ने के लिए लोग बेचैन हों मेरी जानकारी में कोई एक नहीं है, इस बीते दो दशक में। जो पढ़ने के लिए लोगों को बेक़रार करे। तड़पा दे। एक समय था कि चंद्रकांता संतति पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। ख़ुद प्रेमचंद उर्दू छोड़ कर हिंदी में आए थे। राही मासूम रज़ा उर्दू प्रकाशकों की तंगदिली से आजिज़ आकर हिंदी में आए। राही ने आधा गांव उपन्यास उर्दू में लिखा था। पाकिस्तान विभाजन के खिलाफ स्वर था आधा गांव का। लेकिन कोई उर्दू प्रकाशक इसे छापने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि उर्दू प्रकाशक भी सांप्रदायिक ही हैं। बहरहाल, आज कथ्य और पठनीयता का जबरदस्त अभाव है हिंदी में। खासकर इन दस बरसों में रचनाओं में प्रतिरोध इतना ज्यादा हो गया है कि प्रतिरोध ही प्रतिरोध रह गया है। रचना गुम हो गई है। रचना गौरैया हो गई है। गौरैया बन कर फुर्र हो गई है।
सवाल- प्रकाशन के नए विकल्प सामने हैं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म हैं। लेखन में एक तरह का खुलापन आया है, इस पर आपका क्या ख्याल है?
-खुलापन पहले भी था, लिखना पहले भी बहुत था पर सोशल मीडिया ने लेखन के ग्राफ को, खुलेपन को बेहिसाब उछाल दे दिया है। अब हर कोई लेखक है, कवि है। जिसे देखिए, पैसा खर्च कर किताब छपवा ले रहा है। लेखक हो, न हो, अब तो जनवादी लेखक संघ भी बढ़िया पुस्तक विमोचन कार्यक्रम पांच सितारा होटलों में करवा रहा है। ख़ूब बढ़िया समीक्षाएं छप रही हैं। लेखक को बहुत कुछ मिल रहा है। उसकी आत्ममुग्धता, उसके ईगो मसाज में गज़ब का इज़ाफ़ा हुआ है। पर पाठक? पाठक तो ख़ाली हाथ दिखता है। प्रकाशक पैसे कमा रहा है। लेखक नाम और यश। लेकिन पाठक चातक प्यास लिए मुंह बाए बैठा है।
सवाल- राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, रवींद्र कालिया सरीखे लेखक अब नहीं रहे। नए लेखकों में इनके करीब किन्हें पाते हैं?
-नए लेखकों में कोई इनके करीब नहीं दिखता है। राजेंद्र यादव और रवींद्र कालिया को हम लेखन के लिए कम, उनके संपादन के लिए ज़्यादा जानते हैं। संस्मरण लेखन के लिए जानते हैं। रवींद्र कालिया की ग़ालिब छुटी शराब लाजवाब है। इसी तरह राजेंद्र यादव की ‘मुड़-मुड़ कर देखता हूं’ भी लाजवाब है। लेकिन इसके प्रतिवाद में जब मन्नू भंडारी ने लिखा कि मुड़-मुड़ कर देखा तो यह भी देखा होता, लिखकर राजेंद्र यादव का सारा गुरूर छीन लिया था। राजेंद्र यादव निरुत्तर थे। बतौर कथाकार राजेंद्र यादव और रवींद्र कालिया बहुत कमज़ोर कथाकार हैं। हां, संपादक दोनों सफल थे। कमलेश्वर कथाकार भी कामयाब थे और संपादक भी। अजब औरा था उनका। एक समय था कि मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव की तिकड़ी बहुत मशहूर थी। इनकी दोस्ती मशहूर थी। पर इसकी सब से कमज़ोर कड़ी राजेंद्र यादव थे। अगर राजेंद्र यादव की ज़िंदगी में हंस न होता, औरतें न होतीं तो कोई उन्हें आज याद भी नहीं करता। औरतें और पत्रिकाएं मोहन राकेश और कमलेश्वर की ज़िंदगी में भी बहुत थीं। सारिका जैसी साधन संपन्न पत्रिका के संपादक रहे दोनों। बारी-बारी। पर हम इन दोनों को इनकी कथा, उपन्यास के लिए भी बहुत जानते हैं। मोहन राकेश तो नाटकों के लिए भी बहुत परिचित हैं। यह तीनों साहित्य और ज़िंदगी में रिस्क लेने के लिए भी बहुत मशहूर रहे हैं।
सवाल- आज के दौर में आपकी नजर में दो अच्छे उपन्यासकार कौन हैं और उनके लेखन में ऐसा क्या है?
-एक शिवमूर्ति, दूसरे सुधाकर अदीब। दोनों की कथा भूमि नितांत अलग है। दोनों का कथ्य और कैनवस भी बहुत अलग है। फकऱ् यह भी है कि शिवमूर्ति के पास गांव, किसान ही बरसों से हैं। शुरू से हैं। किसी कोल्हू के बैल की तरह वह इसी का फेरा लगाने के लिए अभिशप्त हैं। वह इस से बाहर आने की ज़रूरत भी नहीं समझते। कोशिश भी नहीं करते। अभी उनका सौ पात्रों वाला मोटा उपन्यास अगम बहै दरियाव आया है। जबकि सुधाकर अदीब हर बार अपना ही बनाया सांचा तोड़-तोड़ देते हैं। वह चाहे लक्ष्मण के बहाने ‘मम अरण्य’ में राम कथा हो, शाने तारीख़ के बहाने शेरशाह सूरी की कथा हो, कथा विराट के बहाने सरदार पटेल और आज़ादी की कथा, रंग रांची के बहाने मीरा की कथा या फिर आदि शंकराचार्य की कथा के लिए महापथ हो या कश्मीर की ख़ूनी कथा का बयान करती बर्फ और अंगारे।
सवाल- और दो कहानीकार?
-नवनीत मिश्र और हरिचरन प्रकाश। दोनों ज़मीनी लेखक हैं। अपने लेखन को कभी प्रमोट नहीं करते। न किसी संगठन या गैंग में शुमार हैं। नारी मन के अजब चितेरे हैं नवनीत मिश्र।
सवाल- दो नए युवा लेखक जिनमें आपको संभावनाएं दिखती है? उनके लेखन में क्या अलग है?
-योगिता यादव, प्रज्ञा पांडेय। दोनों ही कथ्य और भाषा के स्तर पर बहुत तोड़फोड़ करती मिलती हैं। स्त्री ही नहीं, पुरुष मनोविज्ञान को भी बहुत बारीकी से समझती और समझाती हैं।
सवाल- इस सदी में आलोचना का क्या हाल है? क्योंकि आलोचनाएं अब दिखती नहीं।
-हिंदी में अब आलोचना नाम की संस्था समाप्त है। कह सकते हैं कि एक थी आलोचना।
सवाल- आप वर्तमान साहित्य के सम्पर्क में हैं। नामवर सिंह के जाने के बाद आलोचना के क्षेत्र में उनकी जगह कौन ले सकता है?
-कोई एक नहीं। हिंदी में नामवर इकलौते हैं। न भूतो, न भविष्यति। न मौखिक में, न लिखित में।
सवाल- मौजूदा सदी के आने वाले सालों में डिजिटल साहित्यिक पत्रिकाओं का क्या भविष्य है?
-अब डिजिटल का जमाना है। ऐसे जैसे हसीनों का ज़माना। लेकिन साहित्य पढ़ने का बेस्ट मीडियम प्रिंट ही है, प्रिंट ही रहेगा। डिजिटल नहीं।
सवाल- हिंदी साहित्य के मौजूदा दौर में स्त्री विमर्श को लेकर आपकी क्या राय है?
-भारतीय वांग्मय में स्त्री सर्वदा से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। बावजूद इसके यह स्त्री-विमर्श फर्जी का विमर्श है। षड्यंत्र है, स्त्रियों के खिलाफ़। स्त्री को कमज़ोर करने का विमर्श है। स्त्री-पुरुष समानता की बात होनी चाहिए लेकिन वामपंथियों द्वारा स्त्रियों के शोषण के लिए यह फ़ेमनिस्ट विमर्श साज़िशन चलाया गया। स्त्रियों की देह को गुलाम बनाने के लिए, भोगने के लिए चलाया गया। इस विमर्श की साज़िश में स्त्रियों की देह जितनी उघाड़ी जा सकती थी, उघाड़ी गई है। उघाड़ी जा रही है। इसका शिकार बनी स्त्रियां ख़ुद अपनी देह उघाड़ने को उद्धत मिलती हैं।
सवाल- बेशक यह पहलू ज्यादा हाईलाइट और चर्चित हुआ पर हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श पर गंभीर काम भी हुए हैं?
-सहमत हूं, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं। यह कहने, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि पुरुष और स्त्री बराबर हैं। पर क्या सचमुच? पुरुष प्रधान समाज का बड़ा हल्ला मचाया जाता है निगेटिव अर्थ में। पितृसत्तात्मक समाज की निंदा का जैसे फैशन सा है। पर निर्मम सच यह जानिए कि पुरुष प्रधान समाज में ही स्त्री सुरक्षित मिलती है। इसलिए भी कि किसी हिंसा का जवाब स्त्री प्रति हिंसा से नहीं दे सकती है। पुरुष के मुकाबले स्त्री मानसिक रूप से मजबूत है, शारीरिक रूप से नहीं। आप कल्पना कीजिए कि स्त्री प्रधान समाज में क्या स्त्री इसी तरह सुरक्षित और संरक्षित मिलेगी? फेमनिस्ट आंदोलन और स्त्री-पुरुष समानता दोनों दो बात हैं। पुरुष प्रधान समाज की जगह स्त्री प्रधान समाज की बात पौरुषहीन और कायर समाज के निर्माण की बात करना है। स्त्री विमर्श का पहाड़ा पढ़ने वाले मित्रों से पूछने का मन करता है कि क्या वह जानते हैं कि क़ुरआन में औरतों को पुरुषों की खेती बताया गया है। दुर्भाग्य से मुस्लिम समाज का पुरुष इसे पूरी तरह मानता भी है। इंज्वाय करता है। कोई ऐतराज नहीं है उसे। पुरुषों की इस खेती के खिलाफ़बोलने का साहस किसी स्त्री विमर्शकार में है भला! नहीं है तो स्त्री विमर्श का यह बेहूदा विमर्श बंद कीजिए। सोचिए कि रानी पद्मावती को बीस हज़ार स्त्रियों के साथ जौहर व्रत क्यों करना पड़ा था। आज भी क्या आधी रात को हम अपनी बेटी, बहन,पत्नी या मां को अकेली सड़क पर छोड़ सकते हैं? सच तो यह है कि साहित्य में भी नहीं छोड़ सकते।
सवाल- सिर्फ स्त्री लेखिकाएं क्यों आप जैसे पुरुषवादी मानसिकता के लेखक भी तो यही कर रहे हैं। आपकी कहानी उपन्यासों में क्या स्त्रियों की देह कम उघाड़ा गया है?
-ग़लत बात। स्त्री से प्रेम का वर्णन स्त्री की देह उघाड़ना नहीं है। प्रेम में स्त्री का मन भी होता है हमारी कथाओं और उपन्यासों में। प्रेम एक पवित्र शब्द है। इस प्रेम में मन और देह दोनों ही समाहित हैं। बिना देह के प्रेम पूर्ण नहीं होता। प्रेम एक स्वाभाविक क्रिया है। हमारे यहां इस प्रेम का नैसर्गिक वर्णन है। भावानुभूति है। जीवन है। इसका चटखारा नहीं है। लेकिन अगर कोई लेखिका या लेखक अपनी आत्मकथा में निरंतर अनेक संबंधों का आख्यान रचता जा रहा है, रस ले लेकर चटखारे लेता जा रहा है तो यह उघाड़ना है।
सवाल- तो आप मान रहे हैं कि हंस का स्त्री विमर्श का पूरा आंदोलन ही बेमानी था?
-बिलकुल, आप देखिए न खुद हंस के राजेन्द्र यादव उसका शिकार हो गए। ‘बीमार आदमी के स्वस्थ विचार’ संस्मरणात्मक किताब उन्होंने ज्योति कुमारी के साथ लिखी थी। उसके बाद हुए तमाशे ने राजेंद्र यादव का मान सम्मान तो छीना ही, वे पुलिसिया फंदे में भी आ गए और अंतत: इसी सदमे में जान से हाथ धो बैठे।
सवाल- मौजूदा दौर में दलित चिंतन अचानक से इतना दरिद्र कैसे हो गया?
-हिंदी में यह संपन्न भी कब था। सर्वदा दरिद्रता और कुपोषण ही इसकी ज़िंदगी रही, रहेगी। इसो आरक्षण के संरक्षण के लिए मनुष्यता, समाज और देश को सर्वदा ठेंगे पर रखने के लिए जाना गया है। कोई अपने घर को आग लगाता है भला? यह तो बात-बेबात देश जलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चिंतन के नाम पर हिंसा ही हथियार है इनका। साहित्य में भी आरक्षण के तलबगार लोग कोई चिंतन कैसे कर सकते हैं। साहित्य में भीख मांगकर कोई बड़ा रचनाकार नहीं बन सकता। कोई बड़ी रचना नहीं लिख सकता। एक उदाहरण हैं सुदामा। ब्राह्मण थे पर सर्वदा विपन्न थे। कृष्ण उनके बाल सखा थे। सहपाठी थे। राजा थे। बावजूद इसके वह कृष्ण को मित्र नहीं, परमात्मा मानते थे। लोग भगवान से मांगते हैं पर सुदामा ने कृष्ण नाम के परमात्मा से कभी कुछ मांगा नहीं। मिलने गए भी तो अपने सामथ्र्य भर चावल की पोटली लेकर गए। तो साहित्य भी देने की चीज़ है।
मांगने और लेने की नहीं कि हम तो दलित हैं, हमें अलग से ट्रीट कीजिए। हम प्रवासी हैं, हमें अलग से ट्रीट कीजिए। हमें ज़्यादा दीजिए। हम स्त्री हैं, हमें कुछ ज़्यादा दीजिए। क्यों भाई? ग़लत बात है यह। भारतीय वांग्मय के आदि कवि वाल्मीकि क्या दलित नहीं थे? वेदव्यास क्या दलित नहीं थे? कबीर, रैदास दलित नहीं थे? इन्होंने मांगा कभी अलग से ट्रीटमेंट? उन्हें हम बड़े रचनाकार होने के कारण जानते हैं कि दलित होने के कारण? साहित्य और समाज उन्हें सम्मान नहीं देता? दरअसल दलित चिंतन के पाखंड ने बहुत नुकसान किया है। साहित्य का भी, समाज का भी। नफ़रत और विष बेहिसाब भरा गया है समाज में दलित चिंतन के नाम पर। हिंसक और अश्लील बनाया है। साहित्य सर्वदा मनुष्यता के पक्ष में होता है। वंचित , उपेक्षित और शोषित के पक्ष में होता है। बाकी लोहिया की मानें तो स्त्री भी दलित होती है। वह किसी भी जाति, धर्म या समाज की हो, लेकिन कितने दलित चिंतक इस बात को स्वीकार करते हैं?
सवाल- लेकिन दलित चिंतन एक रिएक्शन है आप ये क्यों भूल जाते हैं। आरक्षण का पूरा फलसफा अलग ट्रीटमेंट पर ही तो आधारित है?
-आरक्षण का फलसफा ही गलत है। नौकरी और राजनीति में ही इस नरक को रहने दीजिए। साहित्य को इस से बख्श दीजिए।
सवाल- क्यों, बख़्श दें? आखिर नौकरी और राजनीति समाज का हिस्सा है और समाज साहित्य का आईना है? आप उस सवर्ण और सुविधा सम्पन्न वर्ग से आते हैं जिन्होंने वह सब नहीं झेला है?
-इसलिए कि साहित्य सब कुछ के बावजूद अभी भी शुचिता पसंद है। नैतिक और मूल्यों को संवर्धित करने के लिए परिचित है। जबकि आरक्षण राजनीति का गंदा खेल है। बहुत गंदा खेल। आप ही बताइए कि क्या अंबेडकर संविधान निर्माता हैं, 389 सदस्यों की संविधान सभा थी। पहले सच्चिदानंद सिन्हा, फिर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो अगर अंबेडकर संविधान निर्माता हैं तो क्या यह बाकी 389 लोग घास छील रहे थे? लेकिन आज हर राजनीतिक पार्टी अंबेडकर को संविधान निर्माता बताते नहीं अघाती है। संविधान सभा की विभिन्न 22 कमेटियां थीं, जिनमें से एक ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे अंबेडकर। बस। लेकिन दलित वोट के लालच ने अंबेडकर को संविधान निर्माता बताकर पूरी संविधान सभा का अपमान करने का सिलसिला सा चल पड़ा है। अंबेडकर तो इस्लाम को कलंक मानते थे। पर मुस्लिम वोट बैंक की लालच में इस बात पर यही राजनीतिक पार्टियां ख़ामोश हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि साहित्य को इससे बख्शिये। इसलिए भी कि यूरोपीय साहित्य में सबार्लटन साहित्य की मुहिम आलरेडी पिट चुकी है।