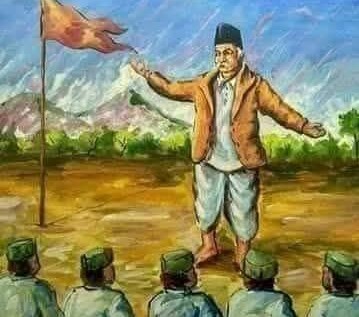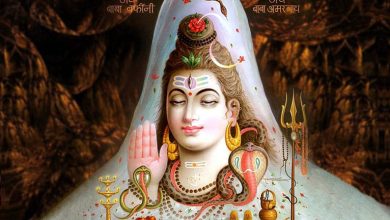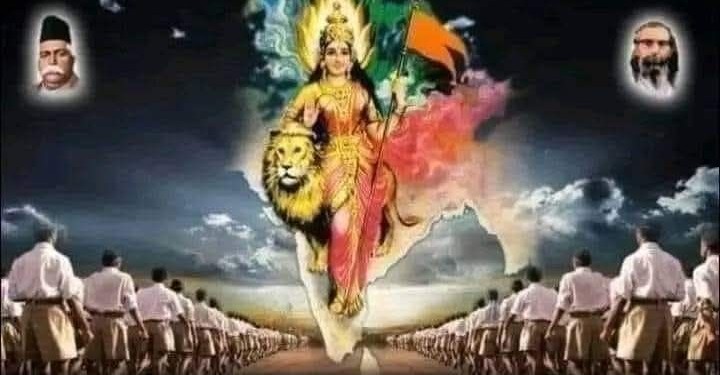
शताब्दी का स्वप्न : समय की रेत पर संघ की अमिट लकीर
राष्ट्र की आत्मा तब ही प्रकट होती है, जब समाज अपने गौरव को पहचानकर भविष्य की ओर बढ़ने का साहस करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सौ वर्ष की यात्रा इसी साहस का विराट आख्यान है। 1925 की पुण्यधरा नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने जिस छोटे से बीज को रोपा था, वह आज वटवृक्ष बनकर भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को आच्छादित कर रहा है। यह केवल संगठन का नहीं, बल्कि उस जीवनदृष्टि का उत्सव है, जो “सर्वे भवन्तु सुखिनः” की वाणी को धरती पर उतारने का संकल्प रखती है। मतलब साफ है यह शताब्दी वर्ष केवल संघ का नहीं, बल्कि एक ऐसे विचार का पर्व है जो “वसुधैव कुटुम्बकम” की भारतीय भावना को जीवन्त रखने की प्रेरणा देता है. या यूं कहे संघ की यह साधना किसी संगठन का निजी अभियान नहीं, भारत की आत्मा का यज्ञ है। यह बताती है कि राष्ट्र का उत्थान न सत्ता के परिवर्तन से आता है, न केवल आर्थिक प्रगति से, बल्कि समाज के अंतःकरण में जागृत उस सामूहिक चेतना से होता है, जो हर व्यक्ति को अपनेपन का अहसास कराए। यही वह पथ है, जिस पर चलते हुए भारत न केवल विश्व को नई दिशा दे सकता है, बल्कि स्वयं अपनी सनातन संस्कृति के आलोक में भविष्य को प्रकाशित कर सकता है। राष्ट्र का वास्तविक उत्थान तभी संभव है, जब हर नागरिक अपने भीतर छिपी सेवा और सद्भावना की लौ को प्रज्वलित करे। संघ की यह साधना उसी दीपशिखा का विस्तार ळे, समय, समाज और नई दृष्टि का।
–सुरेश गांधी
संघ का शताब्दी पर्व केवल संगठन का उत्सव नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का अभिनंदन है। यह उन करोड़ों स्वयंसेवकों के निष्ठा-परिश्रम का सम्मान है, जिन्होंने बिना प्रसिद्धि की आकांक्षा के राष्ट्र को मजबूत करने का काम किया। अखंड भारत का सपना भले अभी भौगोलिक रूप में दूर प्रतीत हो, किंतु सांस्कृतिक अखंडता और आत्मगौरव की लौ पहले से कहीं प्रखर है। मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ संवाद, समावेश और आधुनिकता के संगम पर खड़ा है। यह शताब्दी हमें स्मरण कराती है कि भारत की आत्मा केवल अतीत में नहीं, भविष्य के आकाश में भी चमकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस उजाले को फैलाने वाला दीपस्तंभ है, जो समय की हर आंधी में स्थिर रहकर कहता है : “वसुधैव कुटुम्बकम्कृपूरा विश्व हमारा परिवार है।” राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपने शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहा है। 1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित यह संगठन आज दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी सांस्कृतिक संगठन माना जाता है। सौ साल की इस यात्रा में संघ ने भारतीय समाज, राजनीति, संस्कृति और राष्ट्रजीवन के लगभग हर क्षेत्र को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। यह अवसर केवल संघ के लिए नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए भी एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है।
देखा जाएं तो संघ की स्थापना उस काल में हुई जब स्वतंत्रता आंदोलन का शोर तो था, भारत अंग्रेज़ी हुकूमत से जूझ रहा था और समाज अनेक छिन्न-भिन्नताओं व आतंरिक कमजोरियों से जकड़ा हुआ था। विदेशी शासन से मुक्ति की ज्वाला थी, किंतु जातिगत भेदभाव, धार्मिक संकीर्णता, और सामाजिक कुरीतियां और प्रांतीयता की गांठें उसे कमजोर कर रही थीं। डॉ. हेडगेवार ने इस सच्चाई को समझा, राजनीतिक आज़ादी तभी सार्थक होगी जब समाज भीतर से संगठित और संस्कारित होगा। उसी समझ के अंतर्गत डॉ. हेडगेवार ने एक ऐसे संगठन की नींव रखी, जिसका मूल लक्ष्य “राष्ट्र को संगठित करना” था। शाखा का अनुशासन, सूर्यनमस्कार की ऊष्मा, राष्ट्रगीत की लय, और सामूहिक प्रार्थना की गूंज, यही वह साधना थी जिसने अनगिनत स्वयंसेवकों के हृदय में भारत-भक्ति का तेज भर दिया। स्वतंत्रता संग्राम में संघ का योगदान सीधे राजनीतिक मंच पर न सही, पर राष्ट्रभावना के पोषण में निहित रहा। आज़ादी के बाद का काल संघ के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। गांधीजी की हत्या के बाद लगा प्रतिबंध, कठिन परिस्थितियों में संगठन का पुनरुत्थान, यह सब उसके धैर्य और आत्मविश्वास के परिचायक हैं।
आज संघ केवल शाखाओं तक सीमित नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, गोसेवा, और सांस्कृतिक पुनर्जागरण जैसे अनेक क्षेत्रों में संघ के हजारों सेवा प्रकल्प सक्रिय हैं। मतलब साफ है आज संघ का स्वरूप किसी एक दायरे में नहीं बांधा जा सकता। गंगा से हिमालय तक, अंडमान से अरुणाचल तक, संघ का कार्यक्षेत्र ग्रामोदय से लेकर वैश्विक भारतीय प्रवासियों तक फैला है। शिक्षा में ‘विद्या भारती’, वनवासी कल्याण में ‘वनवासी कल्याण आश्रम’, श्रमिकों के लिए ‘भारतीय मजदूर संघ’, अध्यात्म के लिए ‘विवेकानंद केंद्र’, विज्ञान के क्षेत्र में ‘विज्ञान भारती’, ऐसे हजारों उपक्रम सेवा और संस्कार की ज्योति जला रहे हैं। आपदा के क्षणों में संघ का योगदान अदृश्य पर अत्यंत ठोस रहा है. भूकंप, बाढ़, महामारी, या हाल की कोविड त्रासदी, हर संकट में स्वयंसेवक निःस्वार्थ भाव से राहत और पुनर्वास में लगे रहे। एकल विद्यालयों से लेकर सेवा भारती के चिकित्सा केंद्रों तक, लाखों लोग संघ की इस मौन साधना से लाभान्वित हो रहे हैं।
अखंड भारत : स्वप्न या संकल्प?
संघ के वैचारिक आकाश में ‘अखंड भारत’ केवल भू-राजनीति का मानचित्र नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकात्मता का प्रतीक है। यह स्वप्न उस भारतीय चेतना से उपजा है, जो सिंधु से ब्रह्मपुत्र, काबुल से कांची तक एक ही सांस्कृतिक रागिनी को महसूस करती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देशों से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव इस विचार को आधार देता है। आज की वैश्विक कूटनीति में तत्काल राजनीतिक एकीकरण कठिन भले हो, किंतु सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक निकटता, यही उस स्वप्न का यथार्थ मार्ग है। पड़ोसी देशों में योग, आयुर्वेद, संगीत, साहित्य और साझा इतिहास की गूंज उसी दिशा में संकेत देती है। मतलब साफ है वर्तमान भू-राजनीति में तत्काल राजनीतिक एकीकरण संभव न दिखे, परन्तु सांस्कृतिक एकता और परस्पर सहयोग की दिशा में यह विचार धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है।
संघ का प्रमुख ध्येय : चरित्र से राष्ट्र का निर्माण
संघ का घोष वाक्य स्पष्ट है, “भारत माता को परम वैभव पर प्रतिष्ठित करना।” या यूं कहे “भारत को संगठित, शक्तिशाली और आत्मगौरव से पूर्ण राष्ट्र के रूप में स्थापित करना।” यह राजनीति की सत्ता नहीं, बल्कि समाज के चरित्र व भारतीय संस्कृति का संरक्षण-बढ़ावा निर्माण की साधना है। शाखा केवल व्यायामशाला नहीं, बल्कि व्यक्ति को अनुशासन, स्वावलंबन और सेवा का संस्कार देने का माध्यम है। संघ मानता है कि राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हर नागरिक आत्मगौरव से भरा होगा और विविधता में एकता का भाव अपने भीतर संजोए रखेगा। मतलब साफ है संघ प्रत्यक्ष राजनीति से परे रहकर समाज के हर वर्ग में राष्ट्रीय दृष्टि विकसित करना चाहता है।
मोहन भागवत : परंपरा और नवोन्मेष का संगम
वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत ने संघ की इस शताब्दी यात्रा को नया दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा, “जाति का कोई स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए।” समरसता और संवाद पर उनका विशेष बल है। या यूं कहे संघ ने संवाद और आधुनिकता, दोनों को अपनाया है। उन्होंने सामाजिक समरसता पर विशेष बल दिया, जातिगत भेदभाव मिटाने और सभी धर्मों के बीच संवाद बढ़ाने की पहल की। उनके नेतृत्व में संघ ने पर्यावरण, तकनीक और युवाओं को जोड़ने के नए कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने संघ को केवल परंपरा का संरक्षक न रखकर आधुनिक भारत की चुनौतियों, तकनीक, पर्यावरण, युवाओं की आकांक्षाओं, से जोड़ने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए। विदेशों में भारतीय प्रवासियों से संवाद, विज्ञान और स्टार्टअप संस्कृति से सहभाग, पर्यावरणीय जागरूकता और महिला सहभागिता को प्रोत्साहन, ये सब उनके नेतृत्व में संघ की नयी ऊंचाइयों के प्रतीक हैं। भागवत का दृष्टिकोण यही है कि भारत विश्वगुरु तभी बनेगा जब समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलेगा। वे संघ को केवल परंपरा तक सीमित नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान, शिक्षा और स्टार्टअप संस्कृति से जोड़ने की दिशा में ले जाना चाहते हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों, कॉर्पोरेट जगत और वैश्विक मंचों पर उनके विचारों को गंभीरता से सुना जा रहा है।
भविष्य की राह : चुनौतियां और उम्मीदें
शताब्दी के बाद का काल संघ के लिए अवसर और परीक्षा, दोनों लेकर आएगा। तीव्र शहरीकरण, बदलते सामाजिक समीकरण, डिजिटल क्रांति, आर्थिक विषमताएं, और वैश्विक राजनीति के उतार-चढ़ाव, इन सबके बीच समाज को संगठित रखना आसान नहीं। युवाओं को नैतिकता और राष्ट्रभावना से जोड़ना, धार्मिक-सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना, और पर्यावरण संकट से लड़ना, ये आने वाले समय के प्रमुख प्रश्न होंगे। संघ की शाखाओं से निकली अनुशासन की शिक्षा यदि इन चुनौतियों का समाधान बन सके, तो भारत केवल अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए पथप्रदर्शक होगा। मतलब साफ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष केवल उसके संगठनात्मक विस्तार का उत्सव नहीं है, बल्कि भारतीय समाज के भीतर आत्मचिंतन का भी अवसर है। सौ वर्षों में संघ ने यह सिद्ध किया है कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन और राष्ट्रनिष्ठा से समाज में गहरा परिवर्तन संभव है। अखंड भारत का सपना तत्काल राजनीतिक यथार्थ भले न बने, पर सांस्कृतिक अखंडता और आत्मगौरव की दिशा में संघ का योगदान निर्विवाद है। मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ ने संवाद, समावेश और आधुनिकता को अपनाकर नई ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ाए हैं। आने वाले दशकों में यह देखना रोचक होगा कि संघ अपनी जड़ों को सहेजते हुए वैश्विक भारत के निर्माण में कैसी भूमिका निभाता है। हालिया संवाद में सरसंघचालक मोहन भागवत ने तीन गूढ़ चुनौतियों की ओर संकेत किया, परिवार का क्षरण, अमीरी-गरीबी की गहराती खाई और समाज से घटती सद्भावना। तकनीक की चकाचौंध और व्यक्तिवाद की ठंडी हवा घर की चौखट पर दरारें डाल रही है। जब दुनिया की 76 प्रतिशत संपदा महज 1 प्रतिशत हाथों में सिमट जाए, तो शेष समाज में असंतोष और टकराव का पनपना स्वाभाविक है। भागवत का आग्रह है कि ‘अपनेपन’ की संस्कृति लौटे, मोलजोल का संवाद जीवित हो।

मोहन भागवत : युगबोध के साधक,समरसता के संकल्पी
भारतीय मनीषा ने सहस्रों वर्ष पूर्व उद्घोष किया था, वसुधैव कुटुम्बकम्। संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार मानने का यह भाव केवल शास्त्रीय मंत्र नहीं, बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत का व्यक्तित्व इसी सत्य का मूर्त प्रमाण है। उनका जीवन उस दीप की तरह है जो अंधकार में भी राह दिखाता है, और उस विशाल वटवृक्ष सा है जिसकी छाया में विविधता से भरा समाज समरसता का सुख पाता है। सत्तर का तूफानी दशक, आपातकाल की घनीभूत अंधेरी रात। ऐसे समय में एक युवा ने घर-परिवार का सुख त्यागकर राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित किया। प्रचारक बनकर मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के गांव-गांव में संगठन की ज्योति जलाई। संघ की प्रचारक परंपरा केवल शब्द नहीं, एक तपस्या है, जहां कर्म का अनुशासन व आचरण का तेज ही प्रचार का असली परिचय है। भागवत जी ने इस तपस्या को कर्म की मिट्टी में सींचा और अनुशासन के पुष्पों से सजाया।
सतत साधना की यात्रा
बिहार की गलियों और महाराष्ट्र के विदर्भ की धूलभरी पगडंडियों से लेकर अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख की ज़िम्मेदारी तक, उनका सफर निरंतर साधना का उदाहरण रहा। सन 1925, नागपुर की एक साधारण-सी सुबह। शहर की गलियों में मंद धूप उतर रही थी और हवा में ओस की नमी घुली थी। कुछ किशोर शाखा की पंक्तियों में खड़े सूर्यनमस्कार की लय साध रहे थे। किसी राहगीर के लिए यह दृश्य महज व्यायाम भर रहा होगा, पर डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के लिए यह भविष्य का संकल्प था। उन्होंने देखा कि जिस देश की आत्मा गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हो, उसे मुक्त करने के लिए सबसे पहले उसकी चेतना को जागृत करना आवश्यक है। यही वह बीज था, जो वर्षों बाद वटवृक्ष बनकर काल को चुनौती देगा। संघ का यह सफर आसान नहीं था। सत्ता और समाज, दोनों ओर से उपहास और विरोध के तीर चल रहे थे। 1949 का कानपुर कांग्रेस अधिवेशन इसका सजीव प्रसंग है। जब जुलूस में संघ-विरोधी नारे लगे तो अध्यक्ष पट्टाभि सीतारमैया ने भागीदारी से साफ इंकार किया। यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन संघ अपने पथ से विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसका लक्ष्य शासन प्राप्ति नहीं, समाज का पुनर्निर्माण था। आज वही संगठन चार हजार से अधिक प्रचारकों और साढ़े पाँच लाख से ऊपर स्वयंसेवकों के रूप में सेवा, शिक्षा, ग्राम-विकास, पर्यावरण, आपदा-सहायता और राष्ट्रनिर्माण के विविध क्षेत्रों में सक्रिय है। यह विस्तार केवल संख्या का नहीं, बल्कि दृष्टि का है। संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक उस धागे की तरह है, जो समाज की बिखरी कड़ियों को जोड़ता है। वर्ष 2000 में सरकार्यवाह और 2009 में सरसंघचालक बनने के बाद उन्होंने संगठन को नई दिशा दी। गणवेश परिवर्तन हो या शिक्षा वर्गों में सुधार, संघ की सौ वर्षीय यात्रा में उनका कालखंड परिवर्तन का स्वर्ण अध्याय बन चुका है।
सेवा का अनवरत संकल्प
विश्व महामारी की विषम घड़ी में मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों से कहाकृ“सेवा में संकोच नहीं, सावधानी में ढिलाई नहीं।” उनके मार्गदर्शन में लाखों स्वयंसेवकों ने अन्न, औषधि और उम्मीद का दीप हर ज़रूरतमंद तक पहुँचाया। उनका पंच-परिवर्तन सूत्र, स्वबोध, सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण, सिर्फ संघ का नहीं, सम्पूर्ण मानवता का पथप्रदर्शन है।
संवेदनशील और सृजनशील व्यक्तित्व
भागवत जी का स्वभाव उनके विचारों जितना ही आकर्षक है, मृदु भाषण, गहन श्रवण और सहज संवाद की अद्भुत क्षमता। वे संगीत साधना में रमे रहते हैं, भारतीय वाद्ययंत्रों में निपुण हैं, पठन-पाठन के रसिक हैं। यही संवेदनशीलता उन्हें युवाओं का प्रिय और समाज का विश्वसनीय मार्गदर्शक बनाती है। स्वच्छ भारत से लेकर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और आत्मनिर्भर भारत तक, हर जनांदोलन में उन्होंने संघ की ऊर्जा का संचार किया।

शताब्दी का नया उत्सव
अब जब विजयादशमी 2025 पर संघ अपने शताब्दी वर्ष का उद्घोष करेगा, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के पावन अवसर पर, तब मोहन भागवत का नेतृत्व केवल संगठन का नहीं, पूरे राष्ट्र का भी उत्सव होगा। उनकी जीवन-यात्रा हमें यह संदेश देती है कि राष्ट्रनिर्माण कोई एक दिन का पर्व नहीं, यह निरंतर चलने वाला यज्ञ है। विचार के प्रति अडिग निष्ठा और समय के साथ चलने की सूझबूझ, इन्हीं दो स्तंभों पर नया भारत खड़ा होगा। मोहन भागवत आज के युगबोध के साधक हैं, जहाँ परंपरा और परिवर्तन एक साथ गले मिलते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि समरस समाज और सशक्त राष्ट्र का स्वप्न केवल भाषणों से नहीं, बल्कि निष्ठा, सेवा और सतत कर्म से साकार होता है। यही प्रेरणा हर भारतवासी को अपने भीतर का दीप प्रज्वलित करने का आह्वान करती है।
‘हिंदू’ व हिन्दू राष्ट्र की परिकल्पना
भागवत ने ‘हिंदू’ शब्द को धर्म या जाति की संकीर्ण परिभाषा से बाहर निकाल कर सभ्यता और संवेदना का व्यापक अर्थ दिया। उनके अनुसार यह भूगोल का नहीं, भाव का परिचय है, संस्कृति है, संकीर्णता नहीं। उनका ‘हिंदू राष्ट्र’ किसी सांप्रदायिक राज्य का स्वप्न नहीं, बल्कि ऐसा भारत है जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ विश्वगुरु बनने की क्षमता रखता है। आलोचकों द्वारा बार-बार खींची गई रेखाओं को वे सहजता से मिटा देते हैं। संघ का इतिहास राज्य से टकराव का रहा है, पर समय ने साबित किया कि परिवर्तन सत्ता पलटने से नहीं, समाज की सोच और सामूहिक चेतना के जागरण से आता है। यही असली क्रांति है। यही कारण है कि मुस्लिम और ईसाई समुदायों को साझा विरासत में सहभागी होने का आमंत्रण और जातीय अभिमान व अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि उस पंच-परिवर्तन की प्रस्तावना हैं, जो भविष्य के भारत को गढ़ने में सहायक होगी। आज जब टीवी स्टूडियो का कोलाहल और सार्वजनिक मंचों का शोर विवेक को ढकने की कोशिश करता है, मोहन भागवत का यह विमर्श ताज़ी हवा की तरह है, जिसमें परंपरा की गंध भी है और भविष्य का विश्वास भी। उनकी बातें हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा राष्ट्रवाद वह है, जिसमें सबके लिए स्थान और सबके लिए सम्मान है।
सामूहिक संकल्प
संघ के प्रार्थना में सामूहिक संकल्प का और प्रतिज्ञा में प्रत्येक स्वयंसेवक का व्यक्तिगत संकल्प नित्य प्रतिदिन स्मरण किया जाता है। स्वयंसेवक का अर्थ ही स्वयं से प्रारम्भ करने वाला है। संघ का घटक शब्द का अर्थ है ‘जैसा मैं हूँ, वैसा संघ है और जैसा संघ है, वैसा मैं हूँ’। जैसे समुद्र की हर बूंद समुद्र जैसी है और सब बूंदों से मिलकर ही समुद्र बनता है। यह ‘एक’ और ‘पूर्ण’ का सबंध संघ में प्रारम्भ से ही चल रहा है। स्वयंसेवक का आत्मचिंतन सतत चलता है। सफलता का श्रेय पूरे संघ का होता है। असफलता की स्थिति में ‘मैं कहाँ कम पड़ा’ इसको हर स्वयंसेवक सोचता है। यही प्रशिक्षण स्वयंसेवकों का होता है। यह परिवर्तन की सिद्ध पद्धति है। इसमें कहीं बदल नहीं हुआ है, तब तक तो शाखा का दूसरा मॉडल नहीं है। कार्यक्रम और बाकी सब बदल सकता है। शाखा का समय बदलता है, वेश बदलता है। शाखा में तरह-तरह के कार्यक्रम करने की अनुमति पहले से है, लेकिन शाखा का विकल्प नहीं है। शाखा कभी अप्रासंगिक नहीं होती। आज शाखा मॉडल के बारे में प्रगत देशों के लोग आकर अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। संघ का लक्ष्य है. भारतवर्ष को संगठित और बल संपन्न बनाने का काम 2047 तक सर्वत्र व्याप्त हो जाएगा और चलते रहेगा। समरस, सामर्थ्य संपन्न भारत के विश्व जीवन में समृद्ध योगदान को देखकर सब लोग उसके उदाहरण का अनुकरण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। 1992 में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कहा था कि “इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देखकर दुनिया के अन्यान्य देशों के लोग उस देश का अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा करेंगे। जिससे पूरे विश्व के जीवन में परिवर्तन आएगा”। यह प्रक्रिया 2047 के बाद प्रारम्भ होगी और इसे पूरा होने में 100 वर्ष नहीं लगेंगे। अगले 20-30 वर्षों में यह पूरी हो जाएगी।