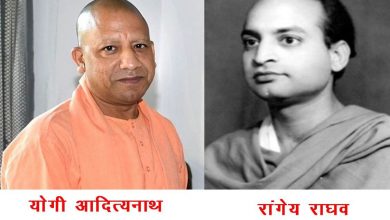पलायन जारी रहा तो लुप्त होंगी भाषाएं

नीरज जोशी
 कुछ वर्ष पूर्व यूनेस्को द्वारा विश्व की भाषाओं पर किये गये सर्वेक्षण में दावा किया गया कि उत्तराखण्ड में सर्वाधिक बोले जाने वाली गढ़वाली एवं कुमाऊंनी भाषाएं विलुप्त हो रही भाषाओं के क्रम में चौथे पायदान पर हैं। सर्वेक्षण मानता है कि उत्तराखण्ड से पलायन का यही क्रम जारी रहा तो 2050 तक ये दोनों भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी। इस सर्वेक्षण में दावा किया गया था कि विश्व में अब तक खत्म हो चुकी छह हजार भाषा बोलियों में 24 बोलियां उत्तराखण्ड की हैं। उत्तराखण्ड मूलत: दो सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक परिवेशों गढ़वाल एवं कुमांऊ में विभक्त है। भाषा के रूप में गढ़वाली एवं कुमाऊंनी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं है। इन भाषाओं की कई उप भाषाओं के साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों मसलन जौनसार, बावर और तराई के थारू, बोक्साओं की अपनी अलग भाषाएं हैं। अभी तक जंगलों में निवास कर रहे वनराजियों की लगभग समाप्ति के कगार पर पहुंच चुकी सबसे पुरानी किराती भाषा की बात की जाए तो कुल मिलाकर उत्तराखण्ड में 13 भाषाएं अपनी कई बोलियों और उप बोलियों के साथ प्रचलन में है। इनमें कुमाऊंनी, गढ़वाली, जाड़, जोहारी, जौनसारी, थारू, बंगाणी, बुक्साड़ी, माच्र्छा, रड़ ल्वू, रवांल्टी और राजी प्रमुख है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ और मूल भाषाएं भारत सरकार के तत्वावधान में गठित की गई पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इंडियन लैंग्वेज (पीएलएसआईएल) ने बताई हैं। जिसने आठ सौ से अधिक भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया है। जिसमें उत्तराखंड में बोली जाने वाली तेरह बोली-भाषाओं का भी सर्वेक्षण किया गया है। इनमें गुजर्री और पर्वतीय भाषाओं को भी मूल माना गया है।
कुछ वर्ष पूर्व यूनेस्को द्वारा विश्व की भाषाओं पर किये गये सर्वेक्षण में दावा किया गया कि उत्तराखण्ड में सर्वाधिक बोले जाने वाली गढ़वाली एवं कुमाऊंनी भाषाएं विलुप्त हो रही भाषाओं के क्रम में चौथे पायदान पर हैं। सर्वेक्षण मानता है कि उत्तराखण्ड से पलायन का यही क्रम जारी रहा तो 2050 तक ये दोनों भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी। इस सर्वेक्षण में दावा किया गया था कि विश्व में अब तक खत्म हो चुकी छह हजार भाषा बोलियों में 24 बोलियां उत्तराखण्ड की हैं। उत्तराखण्ड मूलत: दो सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक परिवेशों गढ़वाल एवं कुमांऊ में विभक्त है। भाषा के रूप में गढ़वाली एवं कुमाऊंनी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं है। इन भाषाओं की कई उप भाषाओं के साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों मसलन जौनसार, बावर और तराई के थारू, बोक्साओं की अपनी अलग भाषाएं हैं। अभी तक जंगलों में निवास कर रहे वनराजियों की लगभग समाप्ति के कगार पर पहुंच चुकी सबसे पुरानी किराती भाषा की बात की जाए तो कुल मिलाकर उत्तराखण्ड में 13 भाषाएं अपनी कई बोलियों और उप बोलियों के साथ प्रचलन में है। इनमें कुमाऊंनी, गढ़वाली, जाड़, जोहारी, जौनसारी, थारू, बंगाणी, बुक्साड़ी, माच्र्छा, रड़ ल्वू, रवांल्टी और राजी प्रमुख है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ और मूल भाषाएं भारत सरकार के तत्वावधान में गठित की गई पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इंडियन लैंग्वेज (पीएलएसआईएल) ने बताई हैं। जिसने आठ सौ से अधिक भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया है। जिसमें उत्तराखंड में बोली जाने वाली तेरह बोली-भाषाओं का भी सर्वेक्षण किया गया है। इनमें गुजर्री और पर्वतीय भाषाओं को भी मूल माना गया है।
गढ़वाली मूलत: गढ़वाल मंडल के सात जिलों में तो कुमाऊंनी कुमाऊं मंडल के छह जिलों में बोली जाती है। तमाम विद्वानों ने गढ़वाली भाषा को छह उपबोलियों बधाणी, सलाणी, जौनसारी, रवांल्टी, श्रीनगरी-बाजारी तथा श्रीनगरी-टिहरियाली आदि में विभक्त किया गया है। कुमाऊंनी को पूर्वी तथा पश्चिमी दो वर्गों में विभक्त किया गया है। पूर्वी कुमाऊंनी के चार उप वर्ग हैं-कुमय्यां, सोर्याली, अस्कोटी तथा सीराली। पश्चिमी कुमाऊंनी के छह उप वर्ग हैं-खसपर्जिया, चौगर्खिया, गंगोली, दनपुरिया, पछाईं और रौं-चौबैंसी। इस तरह कुमाऊंनी की दस उपबोलियां हैं। उत्तराखण्ड में भाषा, संस्कृति के विघटन को लेकर शोर और चिंता कोई नई बात नहीं है। अलग राज्य आंदोलन का सबसे बड़ा मसला पलायन था। यूनेस्को सहित तमाम राष्ट्रीय और राज्य द्वारा भाषाओं पर कराये गये अध्ययन भाषाओं के खतरे के लिए उत्तराखण्ड के पहाड़ों से पिछले पांच दशक से भारी तादाद में हो रहे पलायन को जिम्मेदार मानते है। यह पलायन सिर्फ रोजगार के लिए महानगरों की ओर होने वाला पलायन ही नहीं है बल्कि इसमें नौकरीपेशा या नवधनाढ्य ग्रामीणों का बेहतर सुविधाओं और बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए उत्तराखण्ड के कस्बों में हो रहा पलायन भी है।
उत्तराखण्ड के पहाड़ो में गांव के गांव खाली हो रहे हैं। खेत वीरान पड़े हैं यह सच्चाई अब आम हो चुकी हैं। इस संबंध में उत्तराखण्ड संस्कृति विभाग द्वारा किये गये हालिया सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि राज्य के भाषा चिंतितों की सबसे बड़ी समस्या लिपि है। राज्य में तीन बड़े भाषाई तबकों गढ़वाली कुमाऊंनी और जौनसारी के बीच एक साझा लिपि को लेकर 15 साल में कोई एका नहीं बन पाया। भविष्य में ऐसा संभव भी नहीं है। जौनसारी की एक लिपि कहीं देखने को मिलती है, लेकिन प्रचलन में कम है। गढ़वाली कुमाऊंनी बोलने वाले राष्ट्र की मुख्यधारा के करीब होने के कारण देवनागरी के पक्ष में हैं, उनका मानना है देश के तमाम राज्यों के साथ-साथ जब नेपाली भी देवनागिरी में लिखी जा रही है तो कुमाऊंनी गढ़वाली भाषाओं को क्या परेशानी है। अभी तक इन भाषाओं में खूब सारा लेखन होता रहा है, लेकिन पलायन के चलते इतनी समृद्ध भी नहीं हो पाई कि केन्द्र से इनको अनुसूची में डालने का आग्रह किया जा सके।
कुमाऊंनी गढ़वाली भाषाओं पर खतरा पलायन के चलते उत्पन्न हुआ है। इनके परे बात की जाय तो जौनसारी और बंगाणी भाषाओं पर थोेड़ी सी आधुनिकता और दकियानूसी दिखती है। नई पीढ़ी अपने बच्चों को अंग्रेजीदां देखना चाहती है। जाड़, बोक्सा, थारू बोलने वाले लोग दावा करते हैं कि उनकी संख्या में कहीं कोई कमी नही आई है जबकि बोक्सा और थारू अपनी भाषा बोलने वालों की संख्या में इजाफा बताते हैं। राजी इन सबका अपवाद हैं। क्योंकि वन राजियों की कुल तादाद अब 500 रह गई है। 24 साल पहले इन्हें जंगलों से निकालकर सरकार ने शहरों के बीहड़ों में जो जगह दी उसकी हालात जंगलों से भी बदतर है। इसलिए इनकी भाषा और अस्तित्व दोनों खतरे में हैं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के उच्च हिमालय क्षेत्र में रहने वाले और 1959 से पहले परंपरागत तिब्बत भारत व्यापार में हिस्सा लेने वाले जाड, भोटी, माच्र्छा और तोल्छा भाषा बोलने वाले ज्यादा चिंतित नहीं लगते। उनका मानना है व्यापार के समय से ही उन्हें तिभाषी होना जरूरी होता था, इसलिए उनकी अपनी भाषा सीखना और बोलना नई पीढ़ी के लिए भी जरूरी है। इसके बावजूद भोटी अब कस्बों में बसे कुछ लोगों तक सीमित रह गई है।
ऐसे में सबसे बड़ा खतरा कुमाऊंनी और गढ़वाली भाषाओं को है। यूनेस्को के सर्वे को इस आधार पर सही माना जा सकता है कि उत्तराखण्ड के गांवों से स्थानीय शहरों और महानगरों की ओर पलायन कर चुके लोगों की स्थिति यह है कि उनकी पहली पीढ़ी जो महानगरों में गई मसलन दिल्ली में गढ़वाली कुमाऊंनी बोल और समझ सकती है। दूसरी पीढ़ी समझ सकती है, बोल नहीं सकती और तीसरी पीढ़ी न बोल सकती है और न समझ सकती है।
कमोबेश यही हालात देहरादून, हल्द्वानी जैसे उत्तराखण्ड के बड़े कस्बों के भी हैं। उत्तराखण्ड के गांवों से शहरों और महानगरों की ओर पलायन कर चुके लोगों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक सर्वे या आंकड़ा अभी तक सामने नही आया है। दिल्ली में चुनावी आंकड़े उत्तराखण्ड के प्रवासियों की तादाद 40 लाख के आसपास बताते हैं। इसके अलावा देश के अन्य महानगरों में बसे उत्तराखण्ड के प्रवासियों को लेकर कहा जाता है कि उत्तराखण्ड की आधी आबादी पलायन कर चुकी है। भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण के लिए उत्तराखण्ड की 13 भाषाओं पर काम कर चुके उद्भट विद्वान डाक्टर शेखर पाठक मानते हैं कुल 40 लाख उत्तराखण्ड के प्रवासी महानगरों में बस चुके हैं। इसमें अधिकांश कुमाऊंनी और गढ़वाली बोलने वाले हैं। इस बात में दो राय नही है कि यदि पलायन और अन्य भाषाओं में भागने की यही प्रवृत्ति जारी रही तो कुमाऊंनी और गढ़वाली भाषाओं के साथ-साथ इसके गीत संगीत और साहित्य संस्कृति को भी खतरा हो सकता है। सरकारी और सामाजिक रूप से इस क्षरण को रोकने के प्रयास भी काफी हो रहे है। इन भाषाओं को पाठयक्रम में शामिल करने का बीड़ा भी उठा है, लेकिन पलायन नहीं रुक रहा है। राज्य बनने के 15 वर्ष बाद भी इसकी दर में कमी नही आ रही है। यह घोर चिंता का विषय है राज्य के साथ-साथ केन्द्र को भी इस चिंता से रू-ब-रू होना होगा।