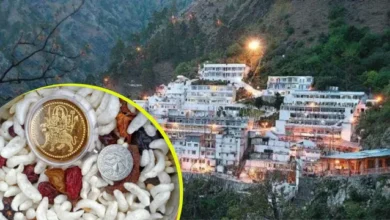21वीं सदी में भारत : कारोबार को लगे पंख

21वीं सदी में भारतीय अर्थव्यवस्था ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। 2010 में पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था ने 1 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा हासिल किया। इस मुकाम पर पहुंचने में आज़ाद भारत को 63 साल का सफर तय करना पड़ा, लेकिन ट्रिगर दब चुका था। अगले सात साल यानी 2017 तक यह दो ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई और फिर तीन साल में यानी 2020 में इसने तीन ट्रिलियन डॉलर का निशान भी पार कर लिया। अर्थव्यवस्था के हैरतअंगेज उतार-चढ़ाव और इस रफ़्तार की दिलचस्प कहानी बता रहे हैं आर्थिक मामलों के जाने-माने विशेषज्ञ आलोक जोशी।
भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछले बीस साल के इतिहास को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। हालांकि पहली नजर में यह आसान है कि किसी भी बीस साल के दौर को दस-दस साल के दो हिस्सों में बांट दिया जाए। लेकिन यहां बात इतनी आसान नहीं है। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार। राजनीति ही नहीं अर्थनीति के मोर्चे पर भी यह विभाजन किसी भी पैमाने पर गलत नहीं ठहराया जा सकता। खासकर अब जबकि सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जबर्दस्त बहस चल रही है कि 2004 से 2014 का दौर भारतीय अर्थनीति का सबसे तेज़ विकास का वक्त था या निरा एक अंधायुग था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही संसद में कहा है कि यह लॉस्ट डिकेड यानी एक खोया हुआ या थोड़ी सख्त भाषा मे कहें तो बर्बाद दशक था यानी आर्थिक मोर्चे पर जो कुछ हो सकता था, उसके मुकाबले यहां सारे मौके गंवा दिए गए। इस मामले पर दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क भी हैं और आस्थाएं भी। मगर विभाजन तक पहुंचने से पहले ज़रूरी है कि बीस साल पहले को पूरी ईमारदारी से याद किया जाए।
2004 वही साल है जब देश में इंडिया शाइनिंग का नारा लगा और अचानक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हार जाने का झटका खासकर व्यापार कारोबार की दुनिया के लिए बहुत बड़ा सदमा था। इस नतीजे का ही असर था कि मुंबई शेयर बाज़ार के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई थी, सेंसेक्स एक दिन में 15.52 फीसदी गिरा था जो तब तक अंकों के लिहाज से सबसे बड़ी गिरावट थी, मगर प्रतिशत में देखें तो आज तक भी बाज़ार किसी एक दिन उससे ज्यादा नहीं गिरा है। यह वाजपेयी सरकार के चुनाव हारने की निराशा थी। लेकिन एक अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने की खबर ने कारोबार जगत के जख्मों पर मरहम का काम किया और बाज़ार फिर चल निकला और ऐसा चला कि 2008 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा संकट का असर आने तक वह लगातार रिकॉर्ड तोड़ता रहा। थोड़े में समझें तो 2003-4 में 3000 के आसपास से चलकर जनवरी 2008 तक सेंसेक्स 21 हजार के पार जा चुका था, यानी सात गुने से ज्यादा। लेकिन उसके बाद मुद्रा संकट का झटका ऐसा लगा कि मार्च तक यह गिरकर वापस साढ़े आठ हज़ार के करीब पहुंच गया। दरअसल अनेक मोर्चों पर यही मनमोहन सिंह के कार्यकाल का सबसे विकट समय था।

रफ़्तार का दौर
अर्थव्यवस्था जबर्दस्त रफ्तार पकड़ रही थी, उद्योगपति और व्यापारी अपना कारोबार फैलाने के लिए जमकर पैसा लगा रहे थे और बाज़ार से कर्ज लेकर लगाने में भी संकोच नहीं कर रहे थे। जैसे तेज़ रफ्तार गाड़ी की दुर्घटना में नुकसान ज्यादा होता है, वैसा ही हाल भारत की अर्थव्यवस्था का भी हुआ। वो तब जबकि भारतीय र्बैंंकग प्रणाली पर इस संकट का लगभग कोई असर नहीं हुआ और आज तक तब के रिजर्व बैंक गवर्नर वाईवी रेड्डी की तारीफ की जाती है कि उन्होंने कितनी समझदारी से भारत पर इस संकट का असर कम से कम होने दिया। लेकिन उसके बाद की परिस्थिति गवाह है कि जितना असर हुआ, गाड़ी को पटरी से उतारने के लिए वो भी काफी था। इसके बावजूद क्या 2004 से 2014 के दौर को बर्बाद दशक कहा जा सकता है? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही बेहतर दे पाएगा। हालांकि यह नहीं भुलाया जा सकता कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा संकट जैसी मुसीबत के बावजूद इन दस वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था सालाना आठ परसेंट की रफ्तार से बढ़ती रही और इस देश का एक बड़ा हिस्सा दस परसेंट से ज्यादा ग्रोथ का सपना भी देखता रहा। शेयर बाज़ार भी इस दौर में आखिरकार करीब पांच गुना होकर बंद हुआ जबकि मोदी सरकार के दस वर्षों में वह करीब तीन गुना ही हो पाया है।
फिर भी बाज़ार या सेंसेक्स के संदर्भ में एक बात रेखांकित करनी जरूरी है कि बीच-बीच में बड़े झटकों के बावजूद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इन बीस वर्षों में तीन हज़ार से चलकर अस्सी हज़ार की ऊंचाई पार कर चुका है यानी करीब छब्बीस-सत्ताईस गुना ऊपर हो गया है। अगर आप लंबे दौर का ग्राफ देखेंगे तो शायद वो तारीखें ढूंढना भी मुश्किल होगा जिन दिनों पर इतिहास की सबसे बड़ी गिरावटें दर्ज हुई हैं। यह बात सेंसेक्स या शेयर बाज़ार पर ही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी लागू होती है। 2004 में भारत का जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद, जिसे अर्थव्यवस्था का आकार भी कह सकते हैं, लगभग सत्तर हजार करोड़ डॉलर था। 2024 में यह पौने चार लाख करोड़ डॉलर या पौने चार ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी थी। थोड़ा और बारीकी से देखें तो 2010 में पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था ने 1 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा हासिल किया। आज़ादी के 63 साल बाद और आर्थिक सुधारों की शुरुआत के भी 19 साल बाद। लेकिन अगले सात साल में 2017 तक यह दो ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई। और फिर तीन साल में यानी 2020 में इसने तीन ट्रिलियन डॉलर का निशान भी पार कर लिया। कोरोना संकट ने इसके बाद फिर एक ब्रेक लगाया लेकिन मोदी सरकार पांच ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने के इरादे पर कायम है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट तो कह रही है कि अगले छह साल तक भारत हर डेढ़ साल में एक ट्रिलियन डॉलर बढ़ाने में कामयाब होगा और 2032 तक भारतीय अर्थव्यवस्था दस ट्रिलियन या दस लाख करोड़ डॉलर की हो चुकी होगी। यह एक रिपोर्ट है और इस पर बहुत से सवाल उठ सकते हैं। इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी चुनौतियों पर अनेक रिपोर्ट मिल सकती हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह लक्ष्य अब बहुत दूर है। भारत दुनिया की तीन बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक है, यह बात अब सपना या दूर की कौड़ी नहीं असलियत है।
जाहिर है इतनी बड़ी इमारत बिना मजबूत नींव के तो बन नहीं सकती। तो अब यह भी देखना चाहिए कि हुआ क्या है, खासकर पिछले बीस वर्षों में। किस सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया और क्या-क्या नहीं होने दिया। यह सारे सवाल हवा में घूम रहे हैं और घूमते रहेंगे। लेकिन सच यह है कि आपस में जबर्दस्त तू-तू मैं-मैं करने वाली इन दोनों पार्टियों की सरकारें आर्थिक मोर्चे पर करीब-करीब एक ही राह पर चलती रही हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनमोहर्न ंसह सरकार ने जो काम शुरु किए थे, मोदी सरकार ने उन्हें न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि कई मामलों में उनमें नई जान भी फूंकी। अब कौन सा दशक बर्बाद रहा और कौन सा आबाद, यह चर्चा शायद तात्कालिक राजनीति में ही ज्यादा काम आने वाली है।

बड़े झटकों से उबरे
यह भी एक बड़े विवाद का मसला है लेकिन आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ा बदलाव 1991 के आर्थिक सुधार ही थे जिन्होंने भारत में निजी उद्योग और कारोबार के लिए बढ़ने का रास्ता खोला। इसके साथ ही एक पूरी पीढ़ी के लिए रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पर पैदा हुए। जिन्हें नौकरियां मिलीं उनको अलग रख दें तब भी ऐसे लोगों की गिनती बहुत बड़ी है जिन्हें अपना कारोबार करने के मौके दिखाई भी पड़े और उन्होंने इन मौकों का फायदा भी उठाया। यह सिलसिला चल तो तभी से रहा था मगर जब इन सुधारों के आर्किटेक्ट मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो मानो उद्यमियों को नई ताकत मिल गई। लोगों को व्यापार कारोबार का हौसला देना ही शायद मनमोहन सिंह सरकार के पहले कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि इस मोर्चे पर एक बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ। विकास की रफ्तार तेज़ थी और उद्यमियों के हौसले बुलंद तो वो जमकर कर्ज भी उठा रहे थे और बैंक बांट भी रहे थे। लेकिन अचानक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा संकट ने खेल बिगाड़ दिया। बहुत सी कंपनियां और कारोबारी अचानक मुसीबत में आ गए। व्यापार में जिस तेजी के भरोसे उन्होंने कर्ज उठाए थे, वो मंदी में बदल गई और उनकी मशीनें, कारखाने, कर्मचारी और ऑर्डर भरने के लिए लिया कच्चा या तैयार माल अचानक उनपर बोझ बन गया। बैंकों के कर्ज खतरे में आ गए। बड़े पैमाने पर छंटनी की खबरें भी आईं और कर्ज डूबने की भी। इसके बावजूद जो कारोबारी और छोटे उद्यमी किसी तरह अपना काम चलाते रहे वो आगे फिर मुनाफे में रहे। लेकिन मूड तो खराब हुआ ही जिसे ठीक होने में बहुत वक्त लग गया और नुकसान भी बहुत हुआ।
इसी तरह का दूसरा बड़ा झटका था मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आई कोरोना महामारी। हालांकि जितना डर था उससे काफी तेज़ी से अर्थव्यवस्था इस संकट से बाहर आई लेकिन नुकसान यहां भी बहुत बड़ा था। अब जाकर कहीं फिर हौसला पुराने मुकाम पर है। इस बीच दो और बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। एक जीएसटी का लागू होना और दूसरा नोटबंदी। इन दोनों के आलोचक कहते हैं कि इनकी वजह से तरक्की की रफ्तार भी कम हुई और लोगों को बेवजह परेशानी भी उठानी पड़ी। लेकिन इन दोनों में भी दोनों सरकारों के बीच तारतम्य का जबर्दस्त उदाहरण दिखता है। जीएसटी लागू करने की कोशिश तो पिछली सरकार के समय से चल ही रही थी और उसे लागू करने के तरीके के अलावा उस पर कांग्रेस की तरफ से कोई आलोचना होती भी नहीं है। आज भी सवाल सिर्फ यही है कि क्या जीएसटी प्रभावी रूप से लागू हो गया है या अब भी दो नम्बर का कारोबार जारी है। लेकिन जीएसटी होना चाहिए और दो नंबर का सारा काम बंद हो जाना चाहिए, इस सिद्धांत पर कोई बहस बाकी नहीं है।

डिजिटल इंडिया
नोटबंदी का मामला थोड़ा अलग है। बिना किसी शक के कहा जा सकता है कि काला धन खत्म करने का जो मकसद नोटबंदी के एलान के वक्त बताया गया था, उसमें यह पूरी तरह नाकाम रही है। सिस्टम में जितनी रकम बताई गई थी, उससे ज्यादा के नोट बैंकों के पास वापस पहुंच गए। यानी किसी का भी काला धन बर्बाद होने की खबर नहीं है। उल्टे आम आदमियों की परेशानी की अनगिनत कहानियां आज भी सुनी सुनाई जा रही हैं। हां, बाद में जब सरकार ने इसे डिजिटल पेमेंट, कैशलेस इंडिया और फाइनेंशियल इनक्लूजन जैसी चीजों से जोड़ दिया तब कह सकते हैं कि अगर नोटबंदी न हुई होती तो शायद डिजिटल लेनदेन इतनी तेज़ी से भारत के कोने-कोने तक नहीं पहुंच पाता। मगर उसमें भी याद रखना चाहिए कि इसके लिए ज़रूरी यूनीक आइडी या आधार कार्यक्रम मनमोहन सिंह सरकार की योजना थी जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने न सिर्फ अपनाया बल्कि उसे काफी ज़ोर-शोर से आगे बढ़ाया। और उसके बाद जीवन के अनेक हिस्सों में डिजिटल प्रभाव जबर्दस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है। यूं भी कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह सरकार के दौर में बहुत से लोगों के भीतर हौसला पैदा हुआ, सरकार ने उस हौसले को पंख दिए और फिर मोदी सरकार ने इस हौसले की उड़ान के लिए ज़रूरी ज़मीन और माहौल यानी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया। हौसला सिर्फ भारतीय उद्यमिता को नहीं मिला।
दुनिया के बड़े उद्योगपतियों को, सरकारों को यह भरोसा दिलाने में भी पिछली सरकार ने बड़ा काम किया कि वो भारत को नजरंदाज़ करके आगे नहीं बढ़ सकते और यह सिलसिला इस दौर में भी जारी है। बल्कि भारत के बड़े-छोटे उद्योगपति अब देश से बाहर कारोबार फैलाने में भी सकुचाते नहीं हैं। विदेशों में कारोबार जमा चुके मित्तल, स्वराज पाल और अनिल अग्रवाल जैसे उद्योगपतियों के अलावा कोरस, जैगुआर लैंड रोवर और नोएलिस जैसी बड़ी कंपनियां अब भारतीय नियंत्रण में हैं और जल्दी ही दुनिया के अनेक देशों में भारतीय ब्रांड भी दिखने लगेंगे, यह कहना अब जल्दबाज़ी नहीं हैं। इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है जो है शेयर बाज़ार में छोटे निवेशकों का दबदबा इस कदर बढ़ना कि अब विदेशी निवेशकों का हौवा गायब सा हो गया है। भारत का मध्यवर्ग न सिर्फ अपने कारोबार की सोचता है बल्कि अगर वो कहीं नौकरी में भी लगा है तो उसे यह समझ आने लगा है कि दूसरे के बड़े कारोबार में छोटा हिस्सा यानी शेयर खरीदकर भी अपना भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है और इसके लिए म्यूचु्अल फंड में छोटी-छोटी किस्तें यानी सिप के रास्ते जो पैसा लग रहा है वो वास्तव में बूंद-बूंद से समुद्र बन चुका है। यह रकम हर महीने अब विदेशी निवेशकों की ताकत और हैसियत को लगातार चुनौती दे रही है। इसी तरह दुनिया के तमाम विकसित देशों में भारतवंशियों की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक हैसियत भी एक दूसरी तरह से भारत की आर्थिक प्रगति में भागीदारी निभा रही है।और यह अभी जल्दी ही कुछ और गुल भी खिला सकती है।

मुफ्तखोरी का युग
एक और बात जो पिछले बीस साल में लगातार चलती और बढ़ती रही वो है जन कल्याण, लाभकारी या लोगों को खुश करने वाली योजनाओं पर बढ़ता खर्च। दोनों ही सरकारों ने ऐसी तमाम योजनाएं चलाई और बढ़ाई हैं। खाने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, किसानों की कर्जमाफी, मनरेगा जैसी योजनाएं पिछली सरकार की थीं तो इस सरकार ने तमाम आलोचनाओं के बावजूद उन्हें आगे ही बढ़ाया है। ऊपर से किसान सम्मान निधि और अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त राशन के बाद अब महिलाओं और नौजवानों को भत्ता देने की भी शुरुआत हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन योजनाओं से समाज के सबसे कमजोर तबकों को लाभ पहुंचा है और सहारा मिला है। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा हो चुका है जो लगातार बड़ा होता जा रहा है। जरूरतमंदों की मदद का यह सवाल तीन सदी पहले अवध के नवाब आसफुद्दौला के सामने भी आया था जिनके बारे में मशहूर है कि ‘जिसको न दे मौला, उसको दे आसफुद्दौला!’ तो वोट के लिए सरकारें आसफुद्दौला बन गईं। टेक्स भरने वाली जनता की जेबों से खैरातें बांटने का दौर शुरू हुआ। दरअसल, सन 1784 में अकाल पीड़ित जनता को राहत देने के लिए नवाब ने योजना बनाई कि वो एक शानदार इमारत बनवाएंगे जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी मदद हो सकेगी।
किंवदंती है कि दिन में यह इमारत बनती थी और रात में इसे गिरवाया जाता था, ताकि ज्यादा लोगों को काम दिया जा सके। रात में इमारत गिराने आने वालों में बहुत से अमीर-उमरा भी होते थे जो मुंह छिपाकर आते थे ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। नवाब का सोचना भी यही था कि काम देने से एक तो लोगों को खैरात लेने की जिल्लत नहीं उठानी पड़ेगी, और दूसरे उन्हें बैठकर खाने की आदत भी नहीं पड़ेगी। यह किस्सा मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के जन्म से करीब सौ साल पहले का है जिन्होंने अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने के लिए ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट बनाने का सिद्धांत दिया है जिनसे लोगों को काम मिले, बाज़ार में खपत बढ़े और अर्थव्यवस्था का चक्का तेज़ी से घूमने लगे। मगर अब सवाल यह है कि जिन लोगों को मुफ्त अनाज, मुफ्त घर, मुफ्त शौचालय, मुफ्त बिजली और ऊपर से हर महीने खाते में कुछ पैसे भी मिलने लगेंगे वो क्यों और कैसे कुछ करने के लिए निकलेंगे? खासकर तब जबकि हर चुनाव के साथ वोटों के लिए ऐसी योजनाओं की फेहिरश्त लंबी होती जा रही हो और इन खर्चों के लिए जो रकम चाहिए वो कमाएगा कौन?
(लेखक एनडीटीवी प्रॉफिट के संपादक हैं।)